समीक्षा : : प्रभात मिलिंद
संदर्भ : अनिल अनलहातु का सद्य प्रकाशित कविता संग्रह ‘बाबरी मस्जिद तथा अन्य कविताएँ‘

..’यही कारण है कि/मेरी कविताएँ अपने/अकेलेपन के कटघरे से होकर/बूमरैंग की भाँति/वापस लौट आती हैं/अपने निभृत एकांत में/मैं जानता हूँ कि/कुछ पढ़े–लिखे बुद्धिमान लोग/नाक–भौं सिकोड़ते उठेंगे/अपने सजे–सजाए ड्राइंग–कक्षों से/और मेरी कविताओं की पंक्तियाँ/जब्त कर ली जायेंगी/काल–कोठरी में डाल दी जायेंगी/कि उन्हें हवा तक न लगे/वरना मोइन–जो–दड़ो के मुर्दों के टीलों/और कालीबंगा की काली चूड़ियों का/क्या जवाब देंगे ??’.. (संग्रह की कविता ‘कालीबंगा की चूड़ियाँ‘ से)
कविताओं में मार्मिक वक्रोक्तियों का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जा सकता है, या तल्ख़ करुणा में बुझी एक पैनी टीस के तज़ुर्बे से होकर गुज़रना क्या और कैसा होता है — अगर इन बारीक़ तकलीफ़ों को महसूस करना हो तो हमारे समय के महत्वपूर्ण और युवा चिंतक–कवि अनिल अनलहातु की कविताएँ पढ़ना हमारे लिए पाठकीय ज़रूरत और ज़िम्मेदारी दोनों ही हैं. ज्ञानपीठ प्रकाशन से उनका सद्य प्रकाशित कविता संग्रह ‘बाबरी मस्जिद तथा अन्य कविताएँ‘ इस बात की पूरी तस्दीक़ करता है. इस संग्रह से गुज़रते हुए हमें समकालीन कविता के स्थापित और रूढ़ भाषिक सौंदर्य और उस सौंदर्य में अंतर्निहित एक उत्तप्त रोमान का अपेक्षित सुख नहीं मिलता. बल्कि इसके विपरीत इनमें मनुष्यता की धंसी–ठगी हुई आँखों से अनवरत निःसृत होते खारे पानी का कसैला–नमकीन स्वाद और सभ्यता के अवरुद्ध कंठ का एक अस्फुट किन्तु चिरन्तन स्वर अवश्य सुनाई पड़ता है. कविताओं के बहाने दरअसल यह संग्रह एक हलफ़नामा है जो कागज़ी विकासों के निर्लज्ज विज्ञापनों, आर्थिक समानताओं के ढोंगों, सामाजिक–संवैधानिक अधिकारों के भुरभुरे रेतघरों और एक आदमी की बुनियादी ज़रूरतों के फ़रेबों के बरक्स ऊपर–ऊपर भर चुके से दिखालाई देते ज़ख्मों के भीतर के बजबजाते मवाद की सड़ांध की ज़ियारत कराता है.
अनिल अनलहातु जब कहते हैं कि ‘मैं एक करुणा में जीता हूँ/मैं एक करुणा को जीता हूँ/मैं जीता नहीं हूँ, हारता हूँ/हारते हुए भी हारता ही हूँ/और हारते हुए ही जीवन जीता हूँ‘ (बाबरी मस्जिद – 1; पृष्ठ -10) तो वस्तुतः वे एक सजग नागरिक–कवि के रूप में हमारे हर्ट–ब्रेक का न केवल एक पीड़ादायक और समग्र वक्तव्य देते होते हैं बल्कि हमारी संपूर्ण मनुष्यता के मामूलीपन को एक ‘निरपराध‘ अपराध–बोध और अवसाद की एक अंधी सुरंग में अनायास धकेल भी रहे होते हैं. उनके कवि के पास कविता के जो प्रयुक्त उपकरण हैं, उनको यदि साहित्येतर न भी माना जाए तो गैरपारंपरिक ज़रूर माना जाएगा. इस दृष्टि से वे पाँच हज़ार साल पुरानी हमारी रक्तस्नात सभ्यता की कथित यात्रा की जघन्य और अमानुषिक प्रवृतियों के शोधक–सर्जकों की नवीनतम प्रतिनिधि कड़ी के रूप में देखे जा सकते हैं.
‘बाबरी मस्जिद तथा अन्य कविताएँ‘ कवि के पैंतालीस कविताओं का प्रथम संग्रह है. इन कविताओं की काव्य–भाषा बेशक़ हिंदी है लेकिन अपने चिंतन–चरित्र में ये वैश्विक कविताएँ हैं. इनके दीर्घ विषय–विस्तार के एक सिरे पर संथाल परगना के उपेक्षित इलाक़ों में रहने वाली वंचित–विपन्न और कमोबेश मशीन बन चुकी एक मकलू मुर्मू है ‘जो भाषा का मतलब आदेश और शब्दों का कटखनापन समझती है‘ और ‘जिसके होठों पर हंसी देखना एक लंबा और उबाऊ इंतज़ार है‘, वहीं दूसरे सिरे पर अभावग्रस्त ग्वाटेमाला में ऐसी ही वंचित–विपन्न औरतों के हक़ों की ख़ातिर लड़ती और इस गुनाह की एवज़ में निर्वासन भोगती रिगोबेर्टा मेंचू है (कविता – मानवीय पीड़ा का ज़िगुरत). पूँजी और नस्लों की बुनियादों पर बने और बंटे हुए समय और समाज में अपनी बेरोक–टोक आवाजाही की तरह ही ये कविताएँ इतिहास, दर्शन, मिथक, विज्ञान और विश्व–साहित्य की परिधियों और परिदृश्यों के आर–पार भी निर्बाध और लगातार विचरती रहती हैं.
इन कविताओं में जहाँ एक तरफ़ मुक्तिबोध और जीवनानंद दास से लेकर पाब्लो नेरुदा और अलबैर कामू जैसे रचनाकारों के अनगिन पात्र और सन्दर्भ मिलते हैं वहीं दूसरी तरफ़ मोइन–जो–दड़ो और मेसोपोटामिया से लेकर इक्कीसवीं शताब्दी की मौज़ूदा आत्ममुग्ध, प्रतिगामी, परपीड़क, अन्तर्संघर्ष, शोषण और प्रतिशोध में गले तक डूबी हुई और आत्मध्वंसक सभ्यताएँ अपनी प्रवंचनापूर्ण संपूर्णता और मिथ्याभिमान के साथ उपस्थित हैं. वैश्विक पीड़ा का प्रकटन इन पंक्तियों में अपने विक्षोभ की पूर्णता में प्रतिध्वनित होता है — ‘सारी ज़िंदगी की जलालत गर्क है/कि धरती का एक इंच, एक कोना नहीं छोड़ा/जहाँ तन कर खड़ा हो सकूँ और/एक बच्चे की मासूम मुस्कुराहट/जज्ब कर लूँ‘ (विद्रोही आत्माएँ ; पृष्ठ – 28).
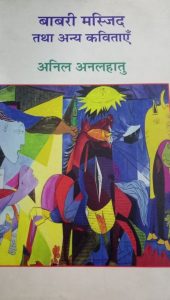
अनिल अनलहातु की पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित कविताओं से होकर गुज़रते हुए बहुधा यह छवि बनती है कि वे मूलतः सन्दर्भों और उद्धरणों के कवि हैं और अपनी बौद्धिक संश्लिष्टता के कारण उनकी कविताएँ एक सामान्य पाठकीय समझ की हद से परे हैं. लेकिन पाठकीय संशय की इस अवस्था के विपरीत छोर से जब हम इन दार्शनिक–ऐतिहासिक–भौगोलिक–समाजशास्त्रीय और मिथकीय सन्दर्भों की पारस्परिकता और आबद्धता को कविताओं से जोड़ कर देखते हैं तब हमें उनके कवि–कर्म की वास्तविक चुनौतियों और लेखकीय उपादेयता का न केवल सम्यक बोध होता है बल्कि तभी हमें उनके रचनात्मक अभीष्ट का सही पता भी मिलता है. सन्दर्भ और उद्धरण अनिल अनलहातु की कविताओं में कदाचित अप्रत्याशित तत्वों की तरह सहजता से दाख़िल होते हैं और तदोपरांत कथ्य की पीड़ाभिव्यक्ति के अनिवार्य एकीकरण का एक कारगर ज़रिया बन जाते हैं. हिंदी कविता के वर्तमान परिदृश्य में यह एक ऐसा विरल गुण है जो या तो अब लुप्त हो चुका है, या अभी–अभी ईज़ाद ही हुआ है. वे अपनी कविताओं में समय और समाज का एक बृहत्तर लोक रचते है जो अपने विस्तार में बिहार के एक पिछड़े और हिंसाग्रस्त जनपद से लेकर भूगोल और इतिहास के अदृश्य–उपेक्षित कोनों तक फैला–पसरा है. इस उपक्रम में इन कविताओं को गोड्डा–दुमका से लेकर कालाहांडी, और दक्षिण अमेरिका से लेकर सुदूर–सघन अफ्रीका के दुर्निवार प्रान्तरों से होते हुए भटकना पड़ता है. संग्रह की कविताओं की अर्थबहुलता और भाषिक प्रयोगधर्मिता के मद्देनज़र अनिल अनलहातु को देशज परंपरा का वैश्विक कवि माना जा सकता है.
कविताई वस्तुतः अनिल अनलहातु के ख़ानाबदोश का एक मुसलसल सफ़रनामा है जो मानव सभ्यता के अलग–अलग कालखण्डों के भग्न वैभवों, अतीत की कपोलकल्पित गौरवगाथाओं और वर्तमान की कौंध भरी वीरानियों का जीता–जागता और बेचैन करने वाला आख्यान है. अपनी स्पष्ट और प्रतिबद्ध संवेदनाओं, व्यापक अध्ययन–संपन्न दृष्टि और गहन चिंतन और अन्वेषण के कारण इन कविताओं का समेकित मूल्यांकन देश–काल के खांचों से परे रख कर ही कर पाना संभव है. संग्रह की पहली ही कविता की आरंभिक पंक्तियों में उनकी रचनात्मकता के इस औचित्य को तलाशा जा सकता है. ‘मैंने अपने को आईने में देखा/न मालूम किस अव्यक्त दुःख से/दुखी हूँ मैं/देख नहीं पाता हूँ/ख़ुद को/कि दिमाग की नसें तड़कती हैं../मैं वर्षों आईना नहीं देखता‘ (बाबरी मस्जिद – 1; पृष्ठ – 9). इसके बावज़ूद ये केवल प्रतिलोम, विग्रह और इति की कविताएँ नहीं अपितु अपनी संभावनाओं में अनुलोम,अनुग्रह और अथ की भी कविताएँ हैं. इनको संवेदना की उसी प्रखरता और वैचारिकी की पक्षधरता के साथ पढ़े जाने की ज़रूरत है जिनके साथ इन्हें रचा गया है. अपने विरल भावों और विंबों में ये सर्वथा नई स्थापनाओं की कविताएँ हैं, और इसीलिए स्वयं से मिलने वालों से ये एक ख़ास और अलग तरह की पाठकीय सलाहियत और तमीज़ की ख्वाहिशमंद हैं.
एली वीजेल ने कहीं लिखा है, ‘यह तो संभव है कि असहायतावश हम अन्याय और पक्षपात को घटित होने से न रोक पाएँ, लेकिन ऐसा कदापि संभव नहीं कि कोई भी सत्ता हमें अन्याय और पक्षपात के प्रतिरोध में आवाज़ उठाने के हक़ से रोक सके.’ धूमिल ने ‘पेशेवर भाषा के तस्कर–संकेतों और बेलमुत्ती इबारतों में अर्थ खोजने की व्यर्थता‘ की बात भी शायद इसी सन्दर्भ में कही है. ‘बाबरी मस्जिद तथा अन्य कविताएँ‘ भी ऐसा नहीं कि समय और समाज की कुत्सित प्रवृतियों और आमजन के नैराश्य का आर्त और विक्षुब्ध एकांतालाप मात्र हैं, बल्कि यह व्यवस्थागत मोहभंग को भी साथ–साथ रेखांकित करती चलती हैं. अपने रचनात्मक प्रयोजन में ये सभ्यता और मनुष्यता के पुनर्निर्माण की फड़फड़ाती नब्ज़ को साफ़–साफ़ महसूस करने की अकुलाहट में आकंठ डूबी हुई कविताएँ हैं.
‘मैं खो रहा हूँ/मैं पा रहा हूँ/मैं ख़त्म हो रहा हूँ/मैं शुरू हो रहा हूँ/मैं खो कर ख़ुद को/ ख़ुद को पा रहा हूँ‘ (नीग्रो जॉर्ज; पृष्ठ – 35) और ‘मैं जमा कर लेना चाहता हूँ/कुछ ऊबे हुए फालतू व निरर्थक/घोषित हो चुके शब्द/क्योंकि यही वह समय है/जब शब्दों की सत्ता और अर्थवत्ता/संदेह के घेरे से/बाहर निकलना चाहती है‘ (डोडो; पृष्ठ – 47) जैसी काव्य–पंक्तियाँ कवि की इसी अकुलाहट को अभिव्यक्त करती हैं. अन्यथा डोडो जैसे निष्कलुष पंछी की तरह ही मूर्ख और निरीह समझी जाने वाली वह हर प्रजाति, सभ्यता, संस्कृति और प्रवृत्ति पूँजी और सत्ता के औज़ारों के ज़रिए एक–एक कर नष्ट कर दी जाएँगी. वह भी फ़क़त इस अदने से कसूर की बिना पर कि वह अहिंसक, सहिष्णु, शान्तिप्रिय, सरल, हानिरहित और निरापद है. कवि की चिंता की ज़द में जहाँ गाँव का बेज़ुबान हरिकिशुना उपस्थित है, वहीं अमेरिकी उपमहाद्वीप में किसी भी तरह जीवित बची रहने के लिए जूझती मय, एज़्टेक, इंका और रेड इंडियन जैसे आदिवासी आबादियाँ भी मौज़ूद हैं. अनिल अनलहातु का कवि विलुप्ति के इन सायास ख़तरों से उन तमाम प्रजातियों की हिफाज़त करना चाहता है जो एक ‘बेलौस हँसी लिए किसी माफ़िया लेखक‘ से लेकर शुभ्रमहल के अंडाकार कक्ष में बैठे ज़हीन दिखते एक सिरफिरे तानाशाह सबके सामूहिक निशानों पर हैं. सत्ता, पूँजी और मज़हब के इतर भी इस दौर में क़ातिलों के कई–कई चेहरे हैं जिनकी शिनाख़्त की ईमानदार कोशिशें ‘बाबरी मस्जिद तथा अन्य कविताएँ‘ करती हैं.
समकालीन कविता के गिने–चुने प्रतिबद्ध कवियों की तरह अनिल अनलहातु की कविताओं में भ्रमभंग का एक सतत अन्तरलाप स्वभावतः अनुस्यूत है. यह भ्रमभंग व्यैक्तिक, संवैधानिक, सांस्थानिक और वैचारिक स्खलन के भिन्न–भिन्न अथवा सामूहिक कारणों से है. यह भ्रमभंग एक ही समय में कवि के मनुष्य और मनुष्य के कवि दोनों का है. कवि की आशंका स्पष्ट है कि ‘सामान्य एक आदमी को/असामान्य बनाकर/मार डालना हमारी/उपलब्धि है‘ (उप्लब्धि ; पृष्ठ – 17). मध्यमवर्ग की वैचारिक तटस्थता और संवेदनात्मक पलायन ने पूँजी और शासन के एकपक्षीय ध्रुवीकरण को पहले से अधिक आसान, स्पष्ट और घातक बनाने में मददगार भूमिकाएँ निभाई हैं. इसीलिए सामाजिक–आर्थिक अधिकारों की समानता इस तथाकथित रूप से परिपक्व लोकतंत्र में अब एक गैरज़रूरी या नाक़ाबिले–ग़ौर मसला है. देश ही नहीं, दुनिया की एक बेशतर आबादी की बुनियादी ज़रूरतें सत्ता और बाज़ार की प्राथमिकताओं में आज कहीं भी दर्ज़ नहीं हैं. सजग–सचेत लोगों को देशद्रोही और पागलों के रूप में सूचीबद्ध किए जाने का काम सुनियोजित तरीक़ों और ज़ोरशोर से ज़ारी है. संग्रह की दूसरी शीर्षक कविता की आरंभिक पँक्तियों में कवि लोकतंत्र के इस फर्जीवाड़े की कलई खोलने को व्यग्र दिखता है – ‘कि लोग मेरी कविताओं की पँक्तियों को पढ़ेंगे/और एकदम से सन्न रह जाएँगे/वे चौंक उठेंगे/और सहमे हुए से/अपने–अपने दड़बों में ढुक जाएँगे/कि बाप जब पढ़ेगा/बेटे की/बेरोज़गार दुःस्वप्नों से दागदार किताब/उसकी झुकी हुई कमर/और झुक जाएगी/कि मेरी कविताएँ/जो अपने समय की नंगी साक्षी होंगी/जला दी जाएँगी/चूल्हों में झोंक दी जाएँगी/कि लोग जब गुज़रेंगे/मेरी कविताओं से होकर/वे भूल जाएँगे/अपने घर का रास्ता/कि ज़िन्दगी पहाड़ पर टँगी लालटेन नहीं है/जो इस घात लगाए समय को ललकार सके.’ इन्ही प्रश्नों में ही वह इनके सांकेतिक उत्तर भी तलाशने की कोशिश करता है – ‘..कि पिछले पाँच हज़ार सालों से/सिंधु घाटी सभ्यता के/ग्रामीण, किसान और मज़दूर/इतिहास में अपनी/जगह माँग रहे हैं/..कि एक सभ्यता के भग्नावशेष/पर खड़ी हुई दूसरी सभ्यता/कब तक सुरक्षित रह पाएगी?’ (बाबरी मस्जिद – 2; पृष्ठ – 12). यह काव्य–पंक्तियाँ मौज़ूदा सियासत की सूरते–हाल और कवि की वैचारिक पक्षधरता दोनों को एक साथ और बिल्कुल साफ़–साफ़ रेखांकित करती हैं. ‘ऑगस्ट क्रांति‘, ‘भारत छोड़ो आंदोलन‘ और ‘हिंदुस्तान पर लदा इंडिया‘ जैसी कविताएँ हमारी विरोधाभासी स्वाधीनता और छद्म लोकतंत्र के भ्रमभंग का आईना हैं.
संग्रह की कविताओं की प्रासंगिकता इनकी अन्तर्वस्तु की सार्वभौमिकता और स्थायित्व में है. अनिल अनलहातु जब ‘एक गुमनाम चिट्ठी बहुत दिनों से भूले एक मित्र के नाम‘ और ‘मिखाइल गोर्ब्याचोव‘ जैसी कविताएँ लिखते हैं तो दरअसल वे मार्क्सवाद के आदर्श दर्शन के व्यवहार रूप में दरकने जैसे सवालों से टकराते होते हैं – ..’इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं/कि मार्क्स के पन्नों से निकला हुआ/बूमरैंग/आ के लगे धड़ाम से/उसी के सीने पर/..चेत जाओ, रुको वहीं पर/और सोचो कि कहाँ भूल/कहाँ चूक हो गई/ब्रह्मांड के मूल में स्थित/द्वैध प्रकृति को समझो/..कि आदमी के भीतर का/कण कब तरंग में रूपायित हो जाएगा/कौन जानता है/और यही कारण है कि/कल तक जो कम्युनिस्ट था/आज एक बुर्ज़ुआ है !!’ (मिखाइल गोर्ब्याचोव ; पृष्ठ – 59). एक समग्र सामाजिक–आर्थिक दर्शन का अपने गैरजिम्मेदार प्रविधियों और बदइंतज़ामी जैसी वज़हों से इतिहास से खारिज़ हो जाना कवि की फ़िक्र में एक बड़े मुद्दे की तरह शामिल है. मार्क्स के सामाजिक–आर्थिक विचारों को अगर सही तरह से आज़माया गया होता तो यह दुनिया बिला शक़ रहने के लिए ज़्यादा बेहतर, मुफ़ीद और महफूज़ जगह होती. टॉलस्टाय के ‘पियरे‘ और ‘अन्ना‘ जैसे किरदारों के जीवन के निजी और एकांतिक अनुभव इसीलिए हमारी स्मृतियों में हमेशा के लिए दर्ज़ हो सके कि उनकी प्रत्यक्ष आबद्धता रूस की स्वाधीनता की पहली लड़ाई और कुलीन वर्ग में नैतिकता के कथित ह्रास जैसे व्यापक सामाजिक सरोकारों से थीं. ‘बाबरी मस्जिद तथा अन्य कविताएँ‘ भी इन अर्थों में सार्वभौम और विशिष्ट हैं.

एक समर्थ कवि भाषा को आज़माता ही नहीं, वह भाषा को रचता और बनाता भी है. अनिल अनलहातु की काव्य–भाषा में भी उनकी अन्वेषक प्रवृति की झलक मिलती है. संग्रह की कविताओं की भाषा अपने आचार–विचार, कहन की त्वरा, बरताव की मौलिकता और अनुभूत प्रभावों के साथ अपने समकाल को असरदार तरीक़े से संबोधित करने में बहुत हद तक समर्थ है. ये कविताएँ वैश्विक परिवर्तन और दबावों के विरूपीकरण के आग्रहों को मानने के साथ–साथ अपनी ज़मीन और जड़ों में विन्यस्त स्थानीयता की गंध का सम्मान करने जैसे दोहरे रचनात्मक दायित्वों का निर्वहन करती चलती हैं. इन कविताओं में स्थान और काल भले बार–बार बदले गए हों, मुखौटे और दृश्यांश भी बदले गए हों. लेकिन युग–युगांतर से यदि कुछ नहीं बदले हैं तो वे हमारी सभ्यता के जीवित पात्र और स्थितियाँ हैं. कवि को अपने पात्र और स्थितियों पर फोकस पर से किसी भी शिफ्टिंग से पूरी तरह गुरेज़ है. और, यही विलक्षणता पाठकों को उसकी काव्य–निष्ठा का विस्मयकारी परिचय देती है. सन्दर्भ हेतु एक छोटी–सी कविता – ‘और ज़िंदा रहने की कोशिश में/ख़ुद को बचाने के लिए/उसने/अपने आप को/वशिष्ठ नारायण सिंह/होने से इनकार कर दिया/कि यह ज़रूरी है/हर आदमी के लिए/गरचे उसे रहना है जीवित/तो/अपने आदमी होने से/ कर दे‘ (इनकार ; पृष्ठ – 56). इस मिडियोकर वक़्त में भिन्न होने का दंड विक्षिप्तता और विस्मृति की क़ीमत पर ही चुकाया जा सकता है. संत्रास और संताप के ऐसे सहज किन्तु त्रासद रूपक पूरे संग्रह में अनायास नमूदार होते रहते हैं. प्रसंगवश ये पंक्तियाँ भी प्रस्तुत हैं – ‘आख़िर क्यों होता है ऐसा/जब चौपाल में चहकता/सोरठा बृजभार गाता/मवेशी धोता/भौजाई से ठट्ठा करता/उत्साह और कर्मठता से लबालब भरा एक आदमी अचानक ठूँठ हो जाता है?/..क्यों उसे सारे मानवीय रिश्ते/बनावटी और खोखले/लगने लगते हैं?/अखिल ब्रह्मांड के/इस अनंत वितान में/क्यों उसे, अपना अस्तित्व/रेत के कण की भाँति/बौना और तुच्छ लगने लगता है‘ (बड़का बाबूजी के प्रति ; पृष्ठ – 99). इसी परिप्रेक्ष्य में यह कहना भी समीचीन होगा कि हिंदी के लिटरेरी एस्टेब्लिशमेन्ट को जिन गिनेचुने युवा नामों से चुनौतियाँ मिल रही हैं, उनमें एक नाम ‘बाबरी मस्जिद तथा अन्य कविताएँ‘ के कवि का भी है.
फ़िलवक़्त जबकि समूची पृथ्वी नवउपनिवेशवाद के धुरंधर जुआरियों के लिए एक कैसिनो में तब्दील हो चुकी है और बाज़ार का बर्चस्व गोड्डा से लेकर अफ्रीका तक बस जीवित बची रहने की क़वायद में मुब्तिला लोगों को ताश के पत्तों की तरह निर्ममता से फेंट और फेंक रहा है, ऐसे सियार समय में हाशिए पर औंधी पड़ी नामुराद आबादी इतनी शाइस्तगी से जिबह की जा रही है कि ख़ुद उसको भी अपने शिकार किए जाने की ख़बर तक नहीं. सौदागरों और दलालों की शातिर नज़रें हमारी जेब के आख़िरी सिक्के पर ही नहीं बल्कि पसीने की आख़िरी बूंद और खून के आख़िरी क़तरे पर हैं. इन प्रतिकूलताओं में ऐसे कविता संग्रह हमें इस अंधेरे–भोथरे समय के आसन्न ख़तरों से आगाह करते हैं. संग्रह का कवि इन कविताओं में बुद्ध से लेकर बाबरी मस्जिद के विध्वंस और उसके बाद की सामाजिक संरचना के बीच के कालखंड की अंतर्यात्रा बार–बार करता है. इस अंतर्यात्रा का निहितार्थ क्या है? उसका सीधा–सीधा सवाल है – ‘जीवन के बिना पर/किसी भी पुरानी ध्वंस सभ्यता के/किसी नमूने की/प्रासंगिकता क्या है?’ (हरिषेण ; पृष्ठ – 67). अतीत की घटनाओं के संदर्भ में सँभवतः कवि के पास एक नई और विकसित समझ है. उसे आभास है कि राजनीति और विचारधारा की तरह कविता भी देश–काल से बद्ध कोई निरपेक्ष विषय नहीं है. उल्लिखित संग्रह की कविताओं को भी तात्कालिकता में पूरी तरह समझ पाना मुमकिन नहीं है और इनका सम्यक मूल्यांकन अतीत–संबद्धता और भविष्य की सँभावनाशीलता को दृष्टि में रख कर ही किया जा सकता है. अनिल अनलहातु वर्तमान में अतीत के हस्तक्षेप का आग्रह भी इस आशा से करते हैं कि अतीत से आए अनुभव और सामर्थ्य के ज़रिए वर्तमान समय और समाज को प्रतिक्रियावादी रूप में इकहरे हो जाने की आशंका को निर्मूल प्रमाणित किया जा सके. मुक्तिबोध, धूमिल और गोरख पांडे से गहरे रूप में प्रभावित होने के बावज़ूद वह सकारात्मक सुझावों और रचनात्मक निर्देशों की संभावनाओं को हमारी सभ्यता और मनुष्यता दोनों के लिए खारिज़ नहीं करना चाहता. संग्रह की कविताएँ शायद इसलिए भी देश और काल के बाहर जाकर भी अपने प्रस्थान–बिंदुओं को पहचानने के लिए बेचैन हैं. यह बेचैनी इन कविताओं के कथ्य और लहजे दोनों को एक बड़ा फलक देती है.
कविता को मन का विलास मानने वालों को संग्रह थोड़ा शुष्क अवश्य प्रतीत हो सकता है. लेकिन समय की इस जर्जर–खुरदरी और काई लगी दीवारों पर उल्लास की रेशम इबारतें लिखना एक मज़ाक सी कोशिश होगी. अनिल अनलहातु इस पारभासक समय के कवि हैं. वह भाषा के वैभव से बाहर निकल कर सभ्यता और मनुष्यता पर छाए धुंधलके को अपनी कविता और विचारों की धार से छांटने की आतुरता से आप्लावित हैं. उनकी कविताओं में जीवन और जिजीविषा दोनों को तलाशने के समान दिखलाई देते हैं. निश्चित रूप से ‘बाबर मस्जिद तथा अन्य कविताएँ‘ हाल–फ़िलहाल के सालों में अपनी तरह का एक विरल कविता संग्रह है. इसे कदाचित आत्ममुक्त होकर पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि इसे पढ़ने के बाद हम वह नहीं रह जाते जो आमतौर पर इसे पढ़ने के पहले हुआ करते थे. कविताओं के बहाने यह हमारे प्रिय पुरखे कवियों के वक्तव्यों का विस्तार है. हो सके तो इन पंक्तियों से प्रतिध्वनित होती अफ़सोस और उम्मीद की दोहरी आवाज़ को ज़रा एक साथ महसूस करने की कोशिश कीजिए – ‘क्या आपको नहीं लगता कि/चीड़ और देवदारु के ये/लंबे और चिकने पेड़/और सुंदर, अच्छे लगते/यदि यह कोहरा–कुहासा हट जाता?/क्या आपको नहीं लगता कि/आप अंधों के संसार में आनेवाले/’नुनेज़‘ हैं?/कि उजाले की दुनिया के बारे में बताना/एक निहायत ही बेतुकी बात थी/कि आपकी भी आँखें निकालने का सुझाव था/ताकि आप भी इनकी ही तरह/कुहरे और कुहासे को/अपनी ज़िंदगी में/उतार लें‘ (कुहरे–कुहासों का देश ; पृष्ठ – 32).
[प्रभात मिलिंद कवि, कहानीकार और समीक्षक हैं.
उनसे prabhatmilind777@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है.]

