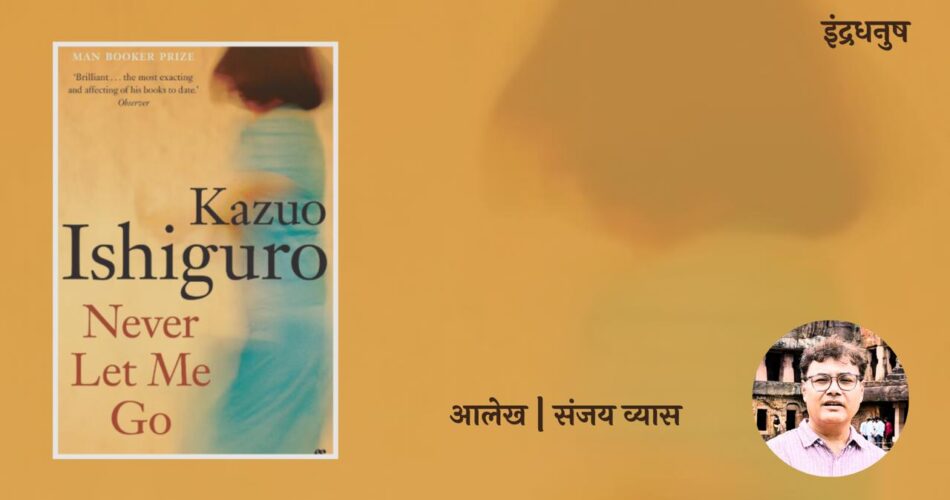आलेख ::
संजय व्यास
कज़ुओ इशिगुरो अपने नोबेल भाषण में ई एम फॉर्स्टर को उद्धृत करते हुए कहते हैं किसी कहानी में पात्र एक समय तक सपाट बने रहते हैं पर जैसे ही वे विश्वसनीय तरीके से पाठक को चौंकाने लगते हैं, वे त्रिआयामी बन जाते हैं। कारण, कि इस प्रक्रिया में उनके कोने ‘गोल’ हो जाते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है जो एक महान लेखक द्वारा सूत्र शैली में कही गई है। इसकी मेरी अपनी टीका यह है कि पात्रों में गहराई या उनमें एक अतिरिक्त विमा उनके व्यवहार के पूर्वानुमान में पाठक के चकित क्रमभंग से आती है। यद्यपि ये पात्र की मनुष्य के रूप में स्थितियों के प्रति उसकी जटिल प्रतिक्रिया से संगति ही है, पर पाठक इसे भांप नहीं पाता।इशिगुरो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसा नहीं होता कि कहानी का पात्र तो त्रिविमीय हो जाए पर उसके सारे संबंध द्विआयामी ही बने रहें?
फ़र्ज़ करें, जैसे गुरु और शिष्य का रिश्ता। क्या ये रिश्ता कुछ नया कह पाता है? या वही थका हुआ स्टीरियोटाइप बन कर रह जाता है? या कि इसी तरह दो प्रतिद्वंद्वी मित्रों का परस्पर संबंध। सवाल होना चाहिए कि क्या इसमें पर्याप्त गतिशीलता है? क्या इसमें कोई भावनात्मक अनुगूंज है?
और इशिगुरो इसी भाषण में कहते हैं– “अचानक मेरे मन में विचार आया कि हर कहानी चाहे वो कितनी ही मौलिक या पारंपरिक रूप से कही गई हो, उसमें उन संबंधों को अनिवार्यतः होना ही होना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, हमें ख़ुशी देते हैं, ग़ुस्सा दिलाते हैं, चौंकाते हैं या हमारे मन को छूते हैं। संभवतः भविष्य में यदि मैं मानवीय संबंधों पर ही ध्यान दूं तो ये पर्याप्त होगा। मेरे पात्र अपना ध्यान स्वयं ही रख लेंगे।”
यहीं से वे अपने अगले उपन्यास ‘नेवर लेट मी गो’ के बारे में संक्षेप में बात करते हैं कि इसे लिखते समय उन्होंने पहले तीन दोस्तों के संबंध-त्रिकोण पर सोचा, उसके बाद अन्य संबंध इसमें से स्वतः प्रकीर्णित होते चले गए। कज़ुओ इशिगुरों का ‘नेवर लेट मी गो’ एक ऐसा उपन्यास है जिसके अनेक पाठ किये गए हैं। कुछ लोगों को ये एक डिस्टोपियन नॉवेल लगता है, कुछ को साई-फाई, कुछ लोग इसे बहुत विचलित करने वाला बताते हैं तो कुछ इसे एक प्रेम कथा कहते हैं। इसका पाठ चाहे कुछ भी हो, उपन्यास अपने विशिष्ट कथानक के कारण आपको झकझोर कर रख देता है। इसे पढ़ना समाप्त करने पर इसके पात्र मानवीय गरिमा से आपकी ओर देखते हैं पर आप उनकी आंखों में केवल उदासी देखते रह जाते हैं।
किताब का मुख्य कथासूत्र इतना अलग है कि जब तक आपको इसके पात्रों का गंतव्य और दिशा का ज्ञान होता है तब तक कहानी में पहले मिले संकेत-शब्द अपने आपको पूरी अर्थ छटा में उद्घाटित नहीं करते। इसलिए मुझे लगता है किताब एकाधिक बार आद्योपांत पाठ की मांग करती है। विशेषकर इसलिए कि ये पाठक को एक जो विरल पाठकीय अनुभव प्रदान करती है जो अवसरों में चुनिंदा और विशिष्टता में एकमात्र जैसा है।

नेवर लेट मी गो [2010] फ़िल्म का एक दृश्य
ये किताब 2005 में आई थी और इस पर बनी फ़िल्म 2010 में। चूंकि मैंने फ़िल्म पहले देखी थी और किताब उसके बहुत बाद में पढ़ी तो पात्रों की यात्रा से पूर्व परिचय होने के कारण मेरे लिए किताब का पहला ही पाठ बेहद सघन था। और दूसरी बार पढ़ने पर तो मैंने अपने आपको पात्रों के और निकट पाया। इसीलिए मैं इसे कम से कम दो बार पढ़े जाने का आग्रह करता हूँ, क्योंकि दूसरी बार आप सांद्रतर अनुभव के कारण और अधिक पुरस्कृत महसूस करेंगे।
इसकी कहानी में जब तक इसके पात्रों की असहायता का पता चलता है, आपको इसके बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आम बच्चों जैसे नज़र आते हैं पर जैसे ही पात्रों का प्रारब्ध आप पर खुलता है, आप बेचैन होना शुरू होते हैं, भीतर से अस्थिर होते जाते है। यद्यपि किताब में शुरू से ही के’रर, डोनैशन, कम्प्लीट होना जैसे शब्द ये संकेत दे देते हैं कि बोर्डिंग स्कूल ‘हेलशैम’ में खिलखिलाते बच्चे एक जुदा भविष्य की तरफ़ ही बढ़ने वाले हैं।
किताब में रिहाइश से बाहर, इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल हेलशैम में बच्चे रहते हैं। ये अपने आप में अलग दुनिया है। ‘स्टूडेंट्स’ हैं, गार्डियन हैं, हैड गार्डियन मिस एमिली हैं, मिस लूसी है, और एक ‘मदाम’ हैं जो कभी कभार अपनी गाड़ी से आती है और अचानक किसी ‘स्टूडेंट’ के सामने पर डर जाती है। बच्चों की ये दुनिया एक ‘बबल’ में हैं जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं हो सकता।
जो इसका डिस्टोपियन पाठ करते हैं उनका तर्क इस किताब की कथावस्तु है जिसके अनुसार हेलशैम में पढ़ने वाले बच्चे असल में क्लोन हैं जो इसलिए इस दुनिया में लाए गए हैं ताकि उनके अंग बीमार लोगों को लगाए जा सकें। वे एक उम्र तक इसी स्कूल में रहेंगे फ़िर सोलह की उम्र में ए ‘कौटेज’ के रूप में बाहर की दुनिया से पहली बार जुड़ेंगे। ‘कौटेज’ तबाह फार्म के बचे खुचे कमरों, बार्न और आउटहाउसेज़ के रूप में हैं। जहां वे एक अपेक्षाकृत स्वायत्त जीवन बिताते हैं। लेकिन केवल कुछ समय तक। उसके बाद उन्हें डोनैशन के लिए तैयार होना हैं। उनमें से कुछ एक अरसे तक अंगदाता के तीमारदार के रूप में भी रह सकते हैं पर आखिर में ये ‘स्टूडेंट्स’ अपने जीवन के यौवन में ही अपने प्रमुख अंग दान कर ‘कम्प्लीट’ हो जाएंगे। यही उनका प्रारब्ध निश्चित किया गया है। ये स्टूडेंट्स कभी बुढ़ापा नहीं देखेंगे, इनके नाती पोते नहीं होंगे, ये अधेड़ भी नहीं होंगे और उससे पहले ही इस संसार से विदा कर दिए जाएंगे।
चिकित्सा विज्ञान ने असाध्य रोगों पर अपराजेय बढ़त प्राप्त कर रुग्ण अंगों के लिए प्रत्यारोपण तकनीक में विजयी छलांग लगा ली है। अब स्वस्थ और युवा अंगों को प्राप्त करने के लिए मानव क्लोन की खेती मनुष्य को एक स्वाभाविक तरीका लग रहा है। ये क्लोन्स अपने बचपन में हेलशैम जैसे स्कूल्स में रहते हैं जिनके संचालक दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि वे पुतले मात्र नहीं हैं, उनमें भी ‘आत्मा’ है।
कज़ुओ इशिगुरो के मन में ये कहानी अपने छितरे हुए अंशों में 1990 से थी पर उन्हें इसका अंत नहीं सूझ रहा था। वे इनके अनिश्चित भविष्य के कारक के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। उन्होंने आणविक आपदा को भी इसके अंत के रूप में सोचा पर एक बार रेडियो पर जैव तकनीक पर कोई कार्यक्रम आ रहा था और अचानक उन्हें लगा, कहानी के सारे टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे हैं। जिगसॉ पज़ल, जिसका हल उन्हें मिल गया था। और फ़िर ये किताब इस रूप में आ पाई।
किन्तु इशिगुरो इस कहानी को ‘डार्क’ नहीं मानते। बल्कि वे इसे काफी ख़ुशनुमा कहते हैं। और इसकी वजह है इसके पात्रों, जिनमें तीन प्रमुख हैं, का सकारात्मक मानवीय भावों से युक्त होना। उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण और अपनी तय सीमाओं में रहने की असहायता के बावजूद, मनुष्य होने की गरिमा से दिपदिपाते रहना। उनमें चाहनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, ईर्ष्याएं हैं। मूक क्रोध तो है, पर हिंसा नहीं है, आक्रामकता नहीं है। वे जानते हैं उन्हें छीजते रहना है, भागना उनके लिए विकल्प नहीं। वे असहाय हैं पर फ़िर भी कम प्राप्त जीवन को अधिकतम में जीना चाहते हैं। और किताब का यही मूल भाव है, यही इसके कथानक का अभीष्ट है।
कैथी और रूथ दोनों टॉमी को चाहती हैं। तीनों उसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। कैथी का स्वभाव संयत, केरींग और ठहराव लिए है जबकि रूथ का स्वभाव अधिकार जताने का है, उसमें ‘वनअपमैनशिप’ का भाव है, वो परिस्थितियों को अपने पक्ष के करने की ज़िद रखती है। टॉमी को दूसरे लड़के बुली करते हैं और इस पर वो चिढ़ता है जिसका परिणाम कि उसका और मज़ाक बनाया जाता है। पर कुछ समय बाद उसके व्यवहार में भी ठहराव आता है। एक क़िस्म का गांभीर्य। कैथी को इसका कारण पता चलता है कि टॉमी को पहली बार महसूस हुआ कि जीवन में कुछ निरुद्देश्यता है जिसे मिस लूसी ने इंगित किया है। बोर्डिंग स्कूल में इन बच्चों को उनके बारे में पर्याप्त नहीं बताया जाता पर बड़े होते रहने पर वो सूचनाओं को विश्लेषित करते हैं और इससे टॉमी को ख़ासी बेचैनी होती है।इन बच्चों को वास्तविकता के बारे में इतना अस्फुट और अपर्याप्त रूप से, कभी गुपचुप तो कभी अफ़वाह की तरह बताया जाता है कि वे एक लगभग आम बचपन से बाहर नहीं आ पाते। उन्हें अधिकतर चित्रकारी, शिल्प या नैतिक पाठ ही पढ़ाए जाते हैं। बोर्डिंग स्कूल के विशाल किन्तु अभेद्य परिसर में लड़के और लड़कियां अलग अलग डॉर्मिटरी में रहते हैं। कम से कम छः के समूह में।
पेंटिंग या अन्य कलाओं में बच्चे अपनी कृतियों को एक जगह रखते हैं जिनमें से कभी कभार विज़िट करने वाली मदाम आकर उनमें से कुछ चुनिंदा नमूने अपनी ‘गैलरी’ के लिए ले जाती है। मदाम द्वारा चुनाव संबंधित बच्चे के लिए गर्व की बात हो जाया करती है।ये बच्चे दिन में फुटबॉल, राउंडर्स जैसे खेल खेलते, अपने दोस्तों के साथ घूमते, संगीत सुनते और रात में अपने अपने शायिका कक्षों में गप्पें मारते हैं।स्कूल से निकलने तक सब अपने बारे में जान चुके होते हैं। सब अपने लिए निरुद्देश्य जीवन की शायद ही चर्चा करते हैं और कॉटेज में वे दोस्ती निभाते, प्रेमियों की तरह रहते अपने छूटे हुए दिनों को याद करते हैं।रूथ टॉमी के साथ रहती है पर जानती है कि टॉमी और कैथी का प्रेम वास्तविक है।
क्रमशः अंगदान कर ‘कंप्लीट’ हो जाने से पहले रूथ कैथी और टॉमी को एक दूसरे से मिलाकर उन्हें मदाम से संपर्क कर कुछ सालों की छूट के लिए याचना का कहती है, ताकि वे दोनों थोड़ा और साथ रह सकें। उन सब ने ‘डिफरल्स’ के रूप में प्रेमियों के लिए ऐसे प्रावधान के बारे में सुन रखा होता है। रूथ उन्हें मदाम के पते की पर्ची देती है जो उसने काफ़ी कोशिशों से मालूम किया होता है। वो टॉमी और कैथी से अपने किए की माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से उन्हें अलग रहना पड़ा।दोनों, टॉमी और कैथी विलंब से प्राप्त परस्पर साथ को रूथ का मैत्री उपहार मानते हैं और इसे सुरक्षित रखने के लिए मदाम के घर जाते हैं।हैलशैम तब तक बंद होकर वीरान हो चुका होता है।घर में मदाम और मिस एमिली उन दोनों को बताती हैं, ऐसा कोई प्रावधान कभी था ही नहीं कि सच्चे प्यार करने वालों को छूट दी जा सके। ये केवल अफवाह भर थी।
कज़ुओ इशिगुरो की कृतियों में स्मृति कहानी की बुनावट का बहुत महत्वपूर्ण रेशा है। उसकी पवित्र उपस्थिति निरंतर बनी रहती है। इशिगुरो स्वयं मानते हैं कि स्मृति अपनी तरह से केलि करती है। यादें कभी चटख तो कभी फीकी होती है, कई बारे ये किनारों से ब्लर होती है, जिससे चित्र में एक विशिष्टता आती है।इस उपन्यास में भी पूरी कहानी कैथी की स्मरण कथा है।इशिगुरो ने उपन्यास में प्रेम के ही एक पक्ष ‘ खो देने ‘ को भी एक सशक्त रूपक के ज़रिए काम में लिया है।हेलशैम में एक दिन कैथी की पसंद की कैसेट जिसमें ‘नेवर लेट मी गो’ गाना होता है, गुम जाती है। तब उसने सुना था कि नॉरफ़क वो जगह हैं जहां इंग्लैंड भर से गुमी हुई चीज़ें लाई जाती हैं। उसकी कैसेट किसी दिन वहां ज़रूर पहुंचेगी और तब उसे वहां ढूंढा जा सकता है।
यही रूपक किताब के आख़िर में इस्तेमाल किया गया है जब चौथे अंगदान के बाद टॉमी ‘कंप्लीट’ हो चुका है। तब कैथी एक बार फ़िर नॉरफ़क जाती है जहां संभवतः वो अपने खोए हुए टॉमी से मिल सकती है। क्योंकि आख़िर नॉरफ़क ही तो वो जगह हो सकती है जहाँ कुछ भी खो चुका पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ हम अपनी गुमशुदा चीज़ों, प्रिय स्मृतियों, अंतरंग रिश्तों को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। कुछ छूट जाने, गुम जाने, खो देने के बाद एक आश्वस्ति बनी रहती है कि इसे कोई एक जगह प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ इशिगुरो ‘लॉस’ के साथ साथ उसके प्रति तड़प, पुनः प्राप्ति की गवेषणा और उसकी कामना के भी रचनाकार हैं।
वो जगह नॉरफ़क क्यों है?
इसे सम्भवतः इस तरह समझा जा सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी नॉरफ़क इशिगुरो की स्मृतियों में टिमटिमाता रहा है। अपने रचनात्मक लेखन के प्रारम्भ को याद करते हुए अपने नोबेल भाषण में वे कहते हैं–
“उस पतझड़ मैं एक पिट्ठू बैग, गिटार और एक पॉर्टेबल टाइपराइटर के साथ बक्स्टन, नॉरफ़क पहुंचा। मुझे ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय में रचनात्मक लेखन के पीजी कोर्से हेतु चुन लिया गया था… इस गांव में एक पुरानी पनचक्की और छितराए खेत थे। लंदन की भागमभाग वाली ज़िंदग़ी के बरक्स यहाँ असामान्य मात्रा में शांति और एकांत था…”
कोई आश्चर्य नहीं कि किताब में गुमशुदा चीज़ों के सही पते के रूप में उन्होनें नॉरफ़क को रखा। वो जगह जो एक डोर के ज़रिये उनसे बंधी रही है। एक जैविक जुङाव वाला स्थान जहाँ उन्होने अपने भीतर के रचनाकार को प्राप्त किया।
किताब से जितना हम गुज़रते हैं उतनी ही किताब हममें से गुज़रती है। ठीक ऐसा ही अनुभव इस पर बनी फ़िल्म नहीं दे पाती। फ़िल्म केवल किताब की हाइलाइट्स, उसकी सुर्खियां ही दिखा पाती है और अंततः केवल किताब का एक साधारण अख़बारी संस्करण बन कर रह जाती है। फ़िल्म किताब में लिखे गये कुछ सम्वादों का प्रयोग ज़रूर करती है जिससे हम कहानी से कुछ सम्बद्धता महसूस कर पाते हैं पर किताब के शब्द जो गझिन और भरी पूरी सृष्टि रचते हैं और जिसका साक्षात्कार बतौर पाठक हमें संतृप्त छोड़ जाता है वो काम फ़िल्म नहीं कर पाती। सम्भवतः इस पर बनी कोई भी फ़िल्म इशिगुरो की इस किताब का वैसा अहसास अपने दर्शक को नहीं दे सकती जैसा ये उपन्यास अपने पाठकों को देता है। इसके शब्द जो सृष्टि करते हैं वो केवल पुस्तकाकार में ही सम्भव है।
इशिगुरो ने लिखित गल्प के वैशिष्ट्य के बारे में लिखा है कि वो अपने पहले उपन्यास ‘अ पेल व्यू ऑफ़ हिल्स’ की सफ़लता से पर्याप्त गर्वित थे पर कहीं न कहीं एक असंतोष का भाव जन्म ले चुका था कि उनकी किताब और उसकी टीवी पटकथा कहानी और शैली में एक जैसे थे। आख़िर फ़िर किताब ही क्यों लिखी जाय जब वैसा ही अनुभव कोई टीवी ऑन कर प्राप्त कर सकता है? और लेखन जब तक कुछ ‘अद्वितीय’ प्रस्तुत न कर पाए तब तक वो कैसे सिनेमा और टीवी जैसे शक्तिशाली माध्यमों के बीच अपने आप को जीवित रख सकता है?यही कारण है कि उनकी ये किताब पाठकों को वो विशिष्ट अनुभव प्रदान करती है जो इस पर बनी इसी नाम की फ़िल्म नहीं कर पाती।
ये कई बार विचार आता है कि इस उपन्यास को पढने के बाद क्यों एक मनुष्य के तौर पर हम अधिक तरलतर हो जाते हैं, क्यों हम उन अभागे पात्रों के प्रति एक भारी कचोट महसूस करते हैं और क्यों हम उनकी ओर आर्द्रता से कातर बने देखते रहते हैं। शायद इसलिये कि इसमें समय भी एक अतिरिक्त विमा है। उन पात्रों के लिये समय ने इतना छोटा अवकाश छोड़ा है कि जिसमें उनकी आकांक्षाओं का विस्तीर्ण आकाश समा नहीं पाता। और सीमित में बद्ध होने की असहायता अपनी पूरी क्लॉस्ट्रोफ़ोबिक घुटन के साथ अंत तक गहरे महसूस होती रहती है, परेशान करती रहती है। इसी अनुभव वैशिष्ट्य के साथ मानवीय संबंधों के सुंदरतम रूप हमारे सामने आते हैं और किताब एक गहरी उदासी के साथ हमें छोड़ जाती है। पात्रों की जीवन को लेकर निर्दोष कामनाएं हमें द्रवित करती हैं, ख़ासकर ये जानकर कि वे अधूरे ही रह जाने के लिए अभिशप्त हैं। पर कैथी, रूथ, टॉमी, सभी जैसे कह रहे हैं, जाने दो, हम इतने में काम चला लेंगे।
•••
संजय व्यास की दो गद्य पुस्तकें ‘टिम टिम रास्तों के अक्स’ और ‘मिट्टी की परात’ प्रकाशित हैं। वे आकाशवाणी जोधपुर में कार्यक्रम निष्पादक हैं और उनसे sanjayvyasjdp@gmail.com पर बात की जा सकती है।