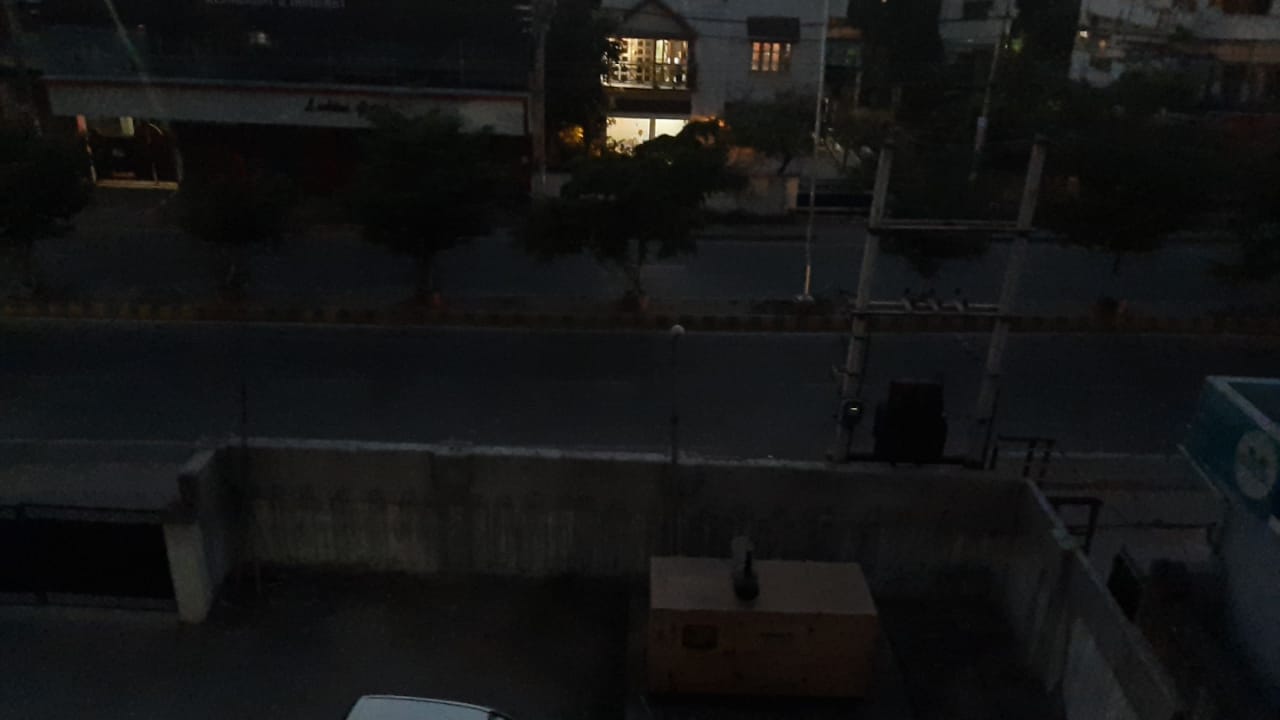नए रास्ते ::
साहित्य और कोरोनाकाल : अंचित

कोरोना और साहित्य के सम्बन्ध में कुछ सीधा कहने और बोलने से बचता रहा था अभी तक. इधर सत्यम ने अपने चैनल के लिए कुछ बोलने की बात की तो मुझको लगा कि थोड़ी बात करनी चाहिए और यह लेख उसी बातचीत के बाद, प्रभात भाई के कहे अनुसार लिख रहा हूँ. जैसा बातचीत में कहा था, बहुत सारे डिस्क्लेमरों के साथ बात करूँगा और जो थोड़ा-बहुत इन दिनों पढ़ता रहा, उसको सिलसिलेवार ढंग से अपने निष्कर्षों के साथ रखने की कोशिश करूँगा.
तो सबसे पहले यही डिस्क्लेमर कि साहित्य कोरोना से जा रही जानों को बचाने या इस महामारी से पैदा हुई दिक़्क़तों को कम करने में कोई सीधी मदद कर सकता है, मुझको नहीं लगता. तो इस समय में साहित्य पढ़ना और लिखना दोनों ही एक प्रिविलेज वाले वर्ग के लिए ही सम्भव है और अपनी उत्पत्ति और अपने कन्सम्प्शन में एक बुर्जुआ काम हो जाता है. और जब यह कार्य सोशल मीडिया पर हो रहा हो, ऐसे लोगों के बीच हो रहा हो, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा है – तो फिर वह अगर हेजेमनी के साथ नहीं भी तो उसके ख़िलाफ़ भी नहीं. तो यह यहीं मान लेना चाहिए कि हम लोग एक बहुत बुर्जुआ काम कर रहे हैं और अपनी असुरक्षाओं की रक्षा इसी साहित्य-जनित विशिष्टता-बोध से करते हैं. स्मृति में दर्ज करने की बात और सत्ता का ध्यान शोषित जनता की तरफ़ खींचने की बात और बाक़ी जनता का ध्यान शोषित जनता की तरफ़ खींचे जाने की बात जैसे तर्क हर रोज़ अब बेमाने होते जा रहे हैं क्योंकि सब इतनी बहुतायत में है और इतने संदर्भों और उल्टे मतों के साथ कि उसका अर्थ बना पाना मुश्किल है. और बदलावों की इस गति से जीत पाना भी. दूसरा डिस्क्लेमर यह कि जो आगे लिखूँगा, निजी राय भर है- अपनी सीमाओं के साथ, और इसे इसी तरह से इग्नोर किया जा सकता है, जिस तरह अमूमन सारी काम की चीज़ें कर दी जाती हैं. बहुत कुछ मुझसे छूट भी गया है. कुछ हिंदी के विवाद वग़ैरह रह गए हों, तो प्रसंग-सहित उनसे अवगत कराया जाए जो आगे उनके बारे में आगे लिखा जा सके.
सबसे ज़्यादा बात ‘उत्तर-जीवन’ पर होने लगी है और यह कि जब यह महामारी चली जाएगी तो स्थितियाँ क्या होंगी. मनुष्य अपने वर्तमान से जब घबराता है, अपने लिए भविष्य में उम्मीद खोजता है. शायद यही बात हमारी प्रजाति को अभी तक विकास की प्रक्रिया में अन्य प्रजातियों से आगे रखती है. शायद ‘एरॉस’ यही है. तो मूलत: दो बातें हो सकती हैं – एक तो इसको मौक़े की तरह देखा जा रहा है कि चीज़ें यहाँ से बेहतरी की तरफ़ बढ़ेंगी और यह परिस्थिति एक रीबूट बटन की तरह काम करेगी. दूसरी सोच यह कि जो है वह और बदतर होगा, पूँजीवाद से पैदा होने वाला शोषण और बढ़ेगा, समाज अधिक बर्बर होगा – किंतु क्या होगा, ये भविष्य के प्रश्न हैं.
जो अभी लिखा जा रहा उसकी बात करूँ तो सबसे पहले मैंने अरुंधती रॉय का लिखा लेख पढ़ा, ‘द पैंडेमिक इज़ अ पोर्टल”. अरुंधती ने बहुत विस्तार से मज़दूरों की स्थिति, उनको लॉकडाउन से होने वाली दिक़्क़तों और उसके पहले जो देश में घट रहा था और जो देश की स्मृति में अब मिट सा गया है, उन दंगों और आर्थिक दिक़्क़तों का विस्तार से ज़िक्र किया है. अमेरिका की स्थिति पर भी वह थोड़ी बात करती हैं. फिर भी अगर मुझे एक पंक्ति निकालनी हो तो मैं वह पंक्ति चुनूँगा जिसमें वे प्रधानमंत्री को “मास्टर ऑफ़ स्पेक्टकल्ज़” कह रही हैं. सम्भवत: इस लेख का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है.
फिर मैंने हरारी का एक लेख पढ़ा जिसमें वे दो सवाल उठाते हैं – सर्विलेंस बनाम निजता और इस महामारी को लेकर राष्ट्रीय बनाम अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता. सर्विलेंस कैसे किया जाए, हरारी इसकी बात करते हैं. बहुत संतुलित भाषा का इस्तेमाल करते हैं. फिर भी इस लेख के लेखक को थोड़ी बू तो आती है. हालंकि हरारी के पक्ष में कहुँ तो निजता और स्वास्थ्य में से चुनाव को वह एक जगह फ़र्ज़ी बताते हैं. आरोग्य-सेतु ऐप्लिकेशन का बार बार लोकेशन माँगना मुझे याद आता रहा. इस सम्भावना से भी उनका इनकार नहीं कि बीमारी के नाम पर सरकारें अपने देशों के नागरिक-डेटा को आपस में साझा करेंगी.
फिर आते हैं जिजेक और जिजेक की बात इधर जब भी होती है मुझे लगता है कि जितनी हड़बड़ी में वह बोलते हुए रहते हैं, उसी हड़बड़ी के साथ वे किताबें भी लिख लेते हैं. कई लेख आ गए. एक पूरी किताब आ गयी और हालंकि वे तमाम सही सवाल पूछते हैं, मुझको जल्दीबाज़ी नहीं समझ आती. यह लगभग हिंदी समाज के लोगों की तरह निष्कर्षों में बात करने की हड़बड़ी है. जैसे यहाँ तुरंत लोगों को महान कवि हर हफ़्ते मिल जाते हैं, हर लेखक अपनी पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ होता है, वैसे ही जिजेक इस फंतासी में जीते हैं कि पूँजीवाद को हटा के साम्यवाद लाया जाएगा और यह होते ही सब सुलझ जाएगा – इस तरह के रिडक्शन पलेमिक कितने हैं और अब्जेक्टिव कितने इसपर क्या बात की जाए. युवा कवि मुकुट को लगता है कि लिखना जिजेक के लिए साँस की तरह है. होगा. फिर भी एक और लेख, “इज़ बार्बरिज़म विद आ ह्यूमन फ़ेस आवर फ़ेट” वाले लेख में वे वही सवाल उठाते हैं जो हमारे देश में बुद्धिजीवी लगातार उठा रहे हैं और जिसके लिए बिना नाम लिए सम्भवत: प्रधानमंत्री ने माफ़ी माँगी है.उनका क्या जो लॉकडाउन अफ़ॉर्ड नहीं कर सकते? इसी लेख में वे इस निष्कर्ष पर भी पहुँचते हैं कि क्या अंत में स्थिति यही रहेगी कि जो लोग किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं उनको तुरंत एक सुखद मृत्यु देकर , सभी संसाधन जिनको बचाया जा सकता है, उनपर केंद्रित किए जाएँ?
यहाँ से हिंदी की ओर चलते हैं. और शायद जो काम का पढ़ा- उसमें सबसे ऊपर अनिल यादव का सदानीरा पर छपा साक्षात्कार है. वैसे तो अनिल ने कई ज़रूरी बातें कहीं, दो बातें उसमें से – एक तो यह कि सरकार तब तक ही ज़िम्मेदारी उठा रही है जब तक किसी तरह की वैक्सीन नहीं निकल जाती. उसके बाद जिसके पास पैसे होंगे वह इलाज कराए और जिसके पास नहीं होंगे वह अपना समझे. यह उतना बहादुरी भरा निष्कर्ष नहीं है जितना अगला है. हिंदी साहित्य का जो समाज है उसपर बात करते हुए वे कहते हैं कि “हिंदी की दुनिया नयी और नक़ली है.उसमें कोई आंतरिक शक्ति अभी नहीं बनी.” मैं कोशिश करूँगा कि इसी नक़ली की विवेचना करूँ – इस नक़ली में अपनी हिस्सेदारी और उसके प्रति और ख़िलाफ़ अपनी ज़िम्मेदारी की विवेचना. हिंदी आचार्यों की भाषा है और उन्हीं के वैलिडेशन से चलती है. जाति-विशेष से या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोगों से मेरा आशय नहीं है. और इसको आप एक आम नियम मानिए कि यह गुण हम सब में पाया जाता है. अनिल यादव की इसी बात पर मेरा विश्वास और पुख़्ता हुआ जब समालोचन पर मैंने प्रचंड प्रवीर का एक लेख पढ़ा. माफ़ करिएगा भैया, थोड़ा भौंडा लगा. जिस तरह प्रकाशक किताब बेचने के लिए बाज़ारू हथकंडे अपना लेते हैं, हिंदी वाले शीर्षक बनाने में भी. कॉलरा में प्यार हुआ था तो कोरोना में भी होना था. बाक़ी अन्य बहुत सारी आलोचना करते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि दो केंद्र मिल कर बाइनेरी बनाते हैं और व्यवहारिकता में सत्ता संघर्ष तमाम मठों को नष्ट करने का नहीं, एक मठ को उठा अपना सिक्का जमाने का संघर्ष भर है.
समालोचन पर ही रश्मि रावत का लिखा एक बहुत सुंदर साहित्यिक टुकड़ा भी पढ़ा और उनको आगे और पढ़ने की इच्छा जगी. मदन सोनी का एक लेख पढ़ा जो ख़ास पसंद नहीं आया. सब स्थगित है – यह भी हेजेमनी के साथ चलता हुआ सा निष्कर्ष है. क्योंकि स्थगन तो सिर्फ़ एक सरकारी आदेश भर है- दुःख जारी हैं, मज़दूरों को पैदल चलना जारी है और लिंचिंग भी जारी है. हिंदू मुस्लिम जारी है. तो “सब” भी जो नहीं आते, उनको ना गिनना भी समस्या है. सुशील कृष्ण गोरे का समालोचन पर छपा लेख भी अच्छा है.कहीं कहीं कुछ व्यंग्य भले हल्के हो जाते हों.
और अंत में कविता की बात. सबसे अच्छी कविताएँ जो इस पूरे साल में पढ़ी हैं, वे हैं सदानीरा पर आयीं अखिलेश सिंह की कविताएँ. इनका आकर्षण अभी भी बरकरार है और गाहे, बगाहे जीवन की बाँसुरियों के बारे में जो कविताएँ हैं उन तक लौटना पड़ता है. देवीप्रसाद मिश्र और संजय कुंदन की कविताएँ भी पढ़ीं और अपने बंधनों के साथ यह उस पीढ़ी की कविताएँ हैं जिसके आगे हिंदी कविता के पास बताने के लिए कांटेंट और फ़ॉर्म के स्तर पर बहुत नया कुछ नहीं है. शायद धैर्य और प्रसिद्धि की आकांक्षा वाली, सूक्तियाँ लिखने वाली पीढ़ी के ठीक पहले के ये आख़िरी लोग हैं. जो फैला बिखरा दूर दूर तक दिखाई देता है वह मुख्यधारा से दूर ही है और कभी-कभार सम्पादकों की कृपा दृष्टि पा लेता है – समझ की सीमा पर बात करना ब्राह्मणवाद लग सकता है सो जय श्री राम.
आख़िरकार, अशोक जी की कविताएँ भी समालोचन पर आयीं. हम अपना समय नहीं लिख पाए. स्वीकार है.
•••
अंचित से anchitthepoet@gmail.com पर बातचीत की जा सकती है. फ़ीचर्ड तस्वीर आसिया ने खींची है.