फागुन के रूप-सौंदर्य को कवियों ने अपनी रचनाओं में बड़ी तत्परता और कुशलता से सहेजा है। होली के रंग से भरे कविताओं के कलेवर से हमारा साहित्य-जगत सम्पन्न तो है ही, यह फागुन के आंतरिक और आँचलिक उत्सव को बड़ी विविधता से चित्रित करता है। आज होली के दिन हम कुछ ऐसी ही रचनाओं पर एक नज़र डालें और उत्सव की वह अनूठी छाप कविताओं में देखें :

ख़ुसरो के शब्दों में-
“…खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूँ पी के संग।
जीत गयी तो पिया मोरे हारी पी के संग।।…”
प्रेम के बंदनवार अमीर ख़ुसरो के आँगन में कुछ यूँ भी दिखाई देते हैं-
“दैया री मोहे भिजोया री
शाह निजाम के रंग में.
कपरे रंगने से कुछ न होवत है
या रंग में मैंने तन को डुबोया री
पिया रंग मैंने तन को डुबोया
जाहि के रंग से शोख रंग सनगी
खूब ही मल मल के धोया री
पीर निजाम के रंग में भिजोया री.”
और भारतेंदु हरिश्चंद्र फागुन के रंग को कुछ ऐसे अंदाज में बयान करते हैं-
“…है रंगत जाफ़रानी रुख अबीरी कुमकुम कुछ है
बने हो ख़ुद ही होली तुम ऐ दिलदार होली में।
रस गर जामे-मय गैरों को देते हो तो मुझको भी
नशीली आँख दिखाकर करो सरशार होली में।”
और कवि पद्माकर के रंग-शब्द कैसे भिगोते हैं फागुन को, ब्रज की गलियों को…
“आई खेलि होरी, कहूँ नवल किसोरी भोरी,
बोरी गई रंगन सुगंधन झकोरै है ।
कहि पदमाकर इकंत चलि चौकि चढ़ि,
हारन के बारन के बंद-फंद छोरै है ॥
घाघरे की घूमनि, उरुन की दुबीचै पारि,
आँगी हू उतारि, सुकुमार मुख मोरै है ।
दंतन अधर दाबि, दूनरि भई सी चाप,
चौवर-पचौवर कै चूनरि निचौरै है ॥”
अपनी सुंदर रचना ‘केशर की कलि की पिचकारी’ में हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला” कहते हैं-
“केशर की, कलि की पिचकारीः
पात-पात की गात सँवारी।
राग-पराग-कपोल किए हैं,
लाल-गुलाल अमोल लिए हैं
तरू-तरू के तन खोल दिए हैं,
आरती जोत-उदोत उतारी-
गन्ध-पवन की धूप धवारी।
गाए खग-कुल-कण्ठ गीत शत,
संग मृदंग तरंग-तीर-हत
भजन-मनोरंजन-रत अविरत,
राग-राग को फलित किया री-
विकल-अंग कल गगन विहारी।”

होली के रंग और गाँव में सरसों के पीले फूलों की दूर तक पसरी छवि कवि हरिवंशराय बच्चन की इस कविता में भलीभाँति मिलती है-
“…अंबर ने ओढ़ी है तन पर
चादर नीली-नीली,
हरित धरित्री के आँगन में
सरसों पीली-पीली,
सिंदूरी मंजरियों से है
अंबा शीश सजाए,
रोलीमय संध्या ऊषा की चोली है।
तुम अपने रँग में रँग लो तो होली है।”
अपने समय में होली के दृश्य को और फागुन की बहार को नज़ीर अकबराबादी कितनी आकर्षक शैली और अपने अनूठे अलहदा अंदाज़ में अपनी इस चर्चित कविता में व्यक्त करते हैं-
“…कुछ तबले खड़कें रंग भरे, कुछ ऐश के दम मुंह चंग भरे
कुछ घुंगरू ताल छनकते हों, तब देख बहारें होली की।
गुलज़ार खिलें हों परियों के और मजलिस की तैयारी हो।
कपड़ों पर रंग के छीटों से खुश रंग अजब गुलकारी हो।
मुँह लाल, गुलाबी आँखें हो और हाथों में पिचकारी हो।
उस रंग भरी पिचकारी को अंगिया पर तक कर मारी हो।
सीनों से रंग ढलकते हों तब देख बहारें होली की।…”
कवि आगे होली के रंग में खुद भी शामिल हो जाते हैं-
“…माजून, रबें, नाच, मज़ा और टिकियां, सुलफा कक्कड़ हो
लड़भिड़ के ‘नज़ीर’ भी निकला हो, कीचड़ में लत्थड़ पत्थड़ हो
जब ऐसे ऐश महकते हों, तब देख बहारें होली की।।”
प्रेम के अन्तस की इतनी गहरी व्याख्या अन्यत्र कहाँ मिलेगी, जैसी मीराबाई के इस उद्गार में हमें प्राप्त होती है-
“फागुन के दिन चार होली खेल मना रे॥
बिन करताल पखावज बाजै अणहदकी झणकार रे।
बिन सुर राग छतीसूं गावै रोम रोम रणकार रे॥
सील संतोखकी केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे।
उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे॥
घटके सब पट खोल दिये हैं लोकलाज सब डार रे।
मीराके प्रभु गिरधर नागर चरणकंवल बलिहार रे॥”

और निराला कुछ पूछ रहे हैं, देखिए-
“मार दी तुझे पिचकारी,
कौन री, रँगी छबि यारी ?
फूल -सी देह,-द्युति सारी,
हल्की तूल-सी सँवारी,
रेणुओं-मली सुकुमारी,
कौन री, रँगी छबि वारी ?…”
लेकिन इस सबके बीच हमारे कवि हुए एक, आप सभी जानते ही होंगे, अरे! हमारे बेढब बनारसी जी, वह देखिए क्या कहते हैं अपने हास्य-रंग में, कैसे मनाए एक संपादक होली!
आफिस में कंपोजीटर कापी कापी चिल्लाता है
कूड़ा-करकट रचनाएँ पढ़, सर में चक्कर आता है
बीत गयी तिथि, पत्र न निकला, ग्राहकगण ने किया प्रहार
तीन मास से मिला न वेतन, लौटा घर होकर लाचार
बोलीं बेलन लिए श्रीमती, होली का सामान कहाँ,
छूट गयी हिम्मत, बाहर भागा, मैं ठहरा नहीं वहाँ
चुन्नी, मुन्नी, कल्लू, मल्लू, लल्लू, सरपर हुए सवार,
सम्पादकजी हाय मनायें कैसे होली का त्यौहार।
कवि का जीवन-गीत फणीश्वर नाथ रेणु की इन पंक्तियों में-
“साजन! होली आई है!
सुख से हँसना
जी भर गाना
मस्ती से मन को बहलाना
पर्व हो गया आज-
साजन! होली आई है!
हँसाने हमको आई है!
साजन! होली आई है!
इसी बहाने
क्षण भर गा लें
दुखमय जीवन को बहला लें
ले मस्ती की आग-
साजन! होली आई है!…”
‘होली हाइकू’ में पूर्णिमा वर्मन अपने विविध शब्द-चित्रों से पाठकों को रूबरू कराती हैं-
अबकी साल
बसंती सपने
तुम ही तुम
कितनी बाट
तके मन फागुन
है गुमसुम
नैनों तलक
फ़हरती सरसों
मन चंदन
ढोल मंजीर
धनकती धरती
चंग मृदंग
टेसू चूनर
अरहर पायल
वन दुल्हन
होली आँगन
मन घन सावन
साजन बिन
बंदनवार
बँधे घर बाहर
बड़ा सुदिन
बिसरें बैर
मनाएँ जनमत
प्रीत कठिन
केसर गंध
उड़े वन-उपवन
मस्त पवन
पागल तितली
भटके दर-दर
बनी मलंग
डाल लचीली
सुबह सजीली
खिले कदंब
छ्प्पन भोग
अठारह नखरे
गया हेमंत

कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ के शब्दों में-
“अरुण दिखलाया बन अरुणाभ।
हो गया मुख प्रभात का लाल।
बने आरंजित पादप पुंज।
रँग गया दिशा सुन्दरी भाल।
गगन मंडल में उड़ा अबीर।
उषा आई पहने पट लाल।
रँगीली होली को अवलोक।
बाल रवि निकला मले गुलाल।”
गोपियाँ क्या अरज कर रहीं होली के दिन श्याम से, घासीराम की इस रचना में कितना सुंदर चित्रित हो रहा है-
“कान्हा पिचकारी मत मार मेरे घर सास लडेगी रे।
सास लडेगी रे मेरे घर ननद लडेगी रे।
सास डुकरिया मेरी बडी खोटी, गारी दे न देगी मोहे रोटी,
दोरानी जेठानी मेरी जनम की बेरन, सुबहा करेगी रे। कान्हा पिचकारी मत मार… ॥1॥
जा जा झूठ पिया सों बोले, एक की चार चार की सोलह,
ननद बडी बदमास, पिया के कान भरेगी रे। कान्हा पिचकारी मत मार… ॥2॥
कछु न बिगरे श्याम तिहारो, मोको होयगो देस निकारो,
ब्रज की नारी दे दे कर मेरी हँसी करेगी रे। कान्हा पिचकारी मत मार… ॥3॥
हा हा खाऊं पडू तेरे पैयां, डारो श्याम मती गलबैया,
घासीराम मोतिन की माला टूट पडेगी रे। कान्हा पिचकारी मत मार… ॥4॥
फागुन का रंग कवि केदारनाथ सिंह की लेखनी से भला कैसे अछूता रह सकता है, वह लिखते हैं-
“गीतों से भरे दिन फागुन के ये गाए जाने को जी करता!
ये बाँधे नहीं बँधते, बाँहें-
रह जातीं खुली की खुली,
ये तोले नहीं तुलते, इस पर
ये आँखें तुली की तुली,
ये कोयल के बोल उड़ा करते, इन्हें थामे हिया रहता!
अनगाए भी ये इतने मीठे
इन्हें गाएँ तो क्या गाएँ,
ये आते, ठहरते, चले जाते
इन्हें पाएँ तो क्या पाएँ।”
कवि श्रीकांत वर्मा कितनी सघनता से फागुन के दृश्य-छाप अपनी इस कविता में भरते हैं-
“फागुन भी नटुआ है, गायक है, मंदरी है।
अह! इसकी वंशी सुन
सुधियां बौराती हैं।
अपनी दुबली अंगुली से जब यह जादूगर
कहीं तमतमायी
दुपहर को छू देता है,
महुए के फूल कहीं चुपके चू जाते हैं
और किसी झुंझकुर से चिड़िया उड़ जाती है।
अह। इसकी वंशी सुन….।।
जब फगुनी हवा कहीं
मोरों के गुच्छ हिला
ताल तलैया नखा तीर पर टहलती है
ऋतु की सुधियां शायद
टेसू बनकर, वन वन
शाख पर सुलगती हैं।
दिन जब टूटे पीले पत्ते सा कांप कहीं
ओझल हो जाता है
संझा जब उमसायी, किसी
ताल-तीर बांस झुरमुट से झांक मुंह दिखाती है,
सरसों के खेतों में पीली
जब एक किरन
गिर गुम हो जाती है,
मेड़ों पर जब जल्दी-जल्दी
कोई छाया
आकुल दिख पड़ती है,
दूर किसी जंगल से मंदरी यह आता है
धिंग धिंग धा धा धिंग धा
धा धिंग धा धा धिंग धा
मांदल धमकाता है,
हौले हौले घर-आंगन में छा जाता है।
इस सूने जीवन में बांसुरी बजाता है।
अह! आह इसकी वंशी सुन…।”
कवि भवानीप्रसाद मिश्र ‘भौरों के दल’ की
‘गुनगुन में अपनी लड़ी गीत की’ मिलाने की बात कुछ इस तरह करते हैं-
“चलो, फागुन की खुशियाँ मनाएँ!
आज पीले हैं सरसों के खेत, लो;
आज किरनें हैं कंचन समेत, लो;
आज कोयल बहन हो गई बावली
उसकी कुहू में अपनी लड़ी गीत की-
हम मिलाएँ।
चलो, फागुन की खुशियाँ मनाएँ!
आज अपनी तरह फूल हँसकर जगे,
आज आमों में भौरों के गुच्छे लगे,
आज भौरों के दल हो गए बावले
उनकी गुनगुन में अपनी लड़ी गीत की
हम मिलाएँ!
चलो, फागुन की खुशियाँ मनाएँ!
आज नाची किरन, आज डोली हवा,
आज फूलों के कानों में बोली हवा,
उसका संदेश फूलों से पूछें, चलो
और कुहू करें गुनगुनाएँ!”

और इन सबके बीच फागुन की सांध्य-बेला बड़े प्रेम से कवि धर्मवीर भारती के शब्दों की खिड़की से कुछ यूँ दृश्यागत होती है-
“घाट के रस्ते
उस बँसवट से
इक पीली-सी चिड़िया
उसका कुछ अच्छा-सा नाम है!
मुझे पुकारे!
ताना मारे,
भर आएँ, आँखड़ियाँ! उन्मन,
ये फागुन की शाम है!
घाट की सीढ़ी तोड़-तोड़ कर बन-तुलसा उग आयीं
झुरमुट से छन जल पर पड़ती सूरज की परछाईं
तोतापंखी किरनों में हिलती बाँसों की टहनी
यहीं बैठ कहती थी तुमसे सब कहनी-अनकहनी
आज खा गया बछड़ा माँ की रामायन की पोथी!
अच्छा अब जाने दो मुझको घर में कितना काम है!
इस सीढ़ी पर, यहीं जहाँ पर लगी हुई है काई
फिसल पड़ी थी मैं, फिर बाँहों में कितना शरमायी!
यहीं न तुमने उस दिन तोड़ दिया था मेरा कंगन!
यहाँ न आऊँगी अब, जाने क्या करने लगता मन!
लेकिन तब तो कभी न हममें तुममें पल-भर बनती!
तुम कहते थे जिसे छाँह है, मैं कहती थी घाम है!
अब तो नींद निगोड़ी सपनों-सपनों भटकी डोले
कभी-कभी तो बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले
ज्यों सोते में किसी विषैली नागिन ने हो काटा
मेरे सँग-सँग अकसर चौंक-चौंक उठता सन्नाटा
पर फिर भी कुछ कभी न जाहिर करती हूँ इस डर से
कहीं न कोई कह दे कुछ, ये ऋतु इतनी बदनाम है!
ये फागुन की शाम है!”
धर्मवीर भारती के शब्द-आँगन से आगे चलने पर हमें झरोखे के उस पार संत-कवि दिखाई दे जाते हैं.
कबीर के लिए फ़ागुन का रंग ‘पिया’ से मिलन की बेला है, जो अपने भीतर इस संसार की माया का रहस्य-दर्पण दर्शाती नजर आती है-
“कोई पिया से मिलावे।
सोई सुंदर जाकों पिया को ध्यान है,
सोई पिया की मनमानी,
खेलत फाग अंग नहिं मोड़े,
सतगुरु से लिपटानी।
इक इक सखियाँ खेल घर पहुँची,
इक इक कुल अरुझानी।
इक इक नाम बिना बहकानी,
हो रही ऐंचातानी।”
कबीर की गली से आगे बढ़ने पर ब्रज के किसी बीच चौराहे आपको रसखान मिल जायेंगे, हाथों में अबीर लिए अपने ही धुन में चिर-अनुरागी-
“फागुन लाग्यौ सखि जब तें, तब तें ब्रजमंडल धूम मच्यौ है
नारि नवेली बचै नहीं एक, विसेष इहैं सबै प्रेम अँच्यौ है
साँझ-सकारे कही रसखान सुरंग गुलाल लै खेल रच्यौ है
को सजनी निलजी न भई, अरु कौन भटू जिहिं मान बच्यौ है।”
गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की अनुभूति हमसे कुछ ऐसे आकर मिलती है-
“वन-वन में फागुन लगा, भाई रे
पात पात फूल फूल डाल डाल
देता दिखाई रे
अंग रंग से रंग गया आकाश गान गान निखिल उदास
चल चंचल पल्लव दल मन मर्मर संग
हेरी ये अवनी के रंग
करते नभ का तप भंग
क्षण-क्षण में कम्पित है मौन
आई हँसी उसकी ये आई रे।”
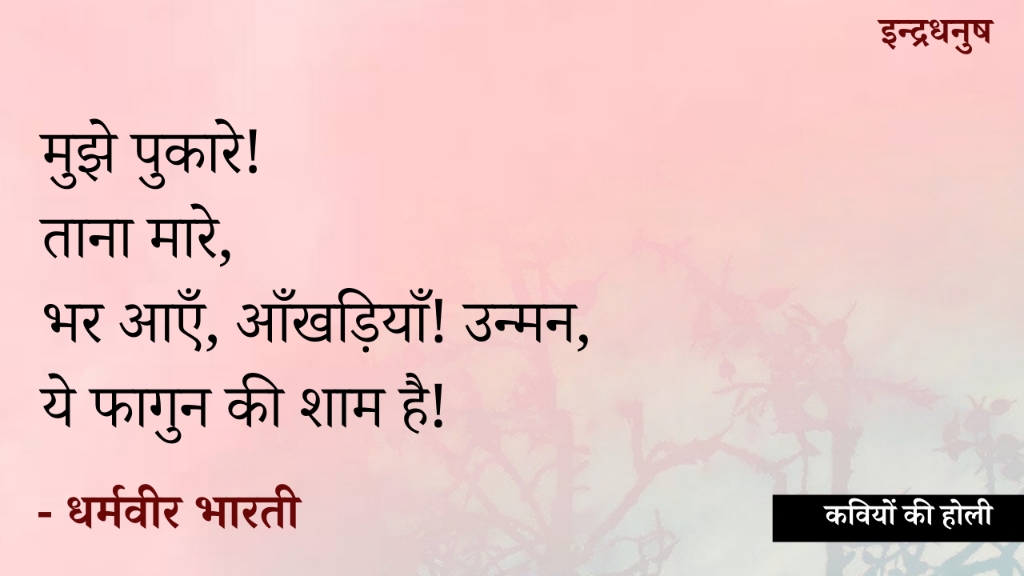
गीतों की बात आए तो चन्द्रसखी की ये रचना आप ढोलक, करताल, झाल और हारमोनियम की सामूहिक जुगलबंदी के साथ फ़ागुन खेलने के माहौल में कुछ यूँ महसूस कर सकते हैं-
“आज बिरज में होरी रे रसिया॥ टेक
होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया॥ आज…
कौन के हाथ कनक पिचकारी,
कौन के हाथ कमोरी रे रसिया॥ आज…
कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी,
राधा के हाथ कमोरी रे रसिया॥ आज…
अपने-अपने घर से निकसीं,
कोई श्यामल, कोई गोरी रे रसिया॥ आज…
उड़त गुलाल लाल भये बादर,
केशर रंग में घोरी रे रसिया॥ आज…
बाजत ताल मृदंग झांझ ढप,
और नगारे की जोड़ी रे रसिया॥ आज…
फेंक गुलाल हाथ पिचकारी,
मारत भर भर पिचकारी रे रसिया।
इतने आये कुंवरे कन्हैया,
उतसों कुंवरि किसोरी रे रसिया। आज…
नंदग्राम के जुरे हैं सखा सब,
बरसाने की गोरी रे रसिया। आज…
दौड़ मिल फाग परस्पर खेलें,
कहि कहि होरी होरी रे रसिया। आज…
कै मन लाल गुलाल मँगाई,
कै मन केशर घोरी रे रसिया॥ आज…
सौ मन लाल गुलाल मगाई,
दस मन केशर घोरी रे रसिया॥ आज…
‘चन्द्रसखी’ भज बाल कृष्ण छबि,
जुग-जुग जीयौ यह जोरी रे रसिया॥ आज…”
तो फागुन अपनी-अपनी तरह से हमारे कवियों की लेखनी में कुछ इस तरह अभिव्यक्त होता है। उनकी आँखों के सामने जब भी कोई अनुभव गुजरता है, उसके स्मृति-चिह्न को हमारे कवि अपने शब्दों में संजोकर रख लेते हैं।
•••
इंद्रधनुष के पाठकों के लिए इन रचनाओं का चयन ‘हिंदी-कविता’, ‘कविता-कोश’ और इंटरनेट के भिन्न-भिन्न वेब-पतों से से साभार यहाँ प्रस्तुत किया गया है। होली की शुभकामनाओं के साथ, हम आशा करते हैं कि पाठक इस चयनित रचना-पाठ से साहित्य में होली की अभिव्यक्ति से परिचित होंगे, एक पुनर्पाठ प्राप्त कर सकेंगे, कवियों की नज़र से फागुन को देख सकेंगे, महसूस कर सकेंगे।– सं.

